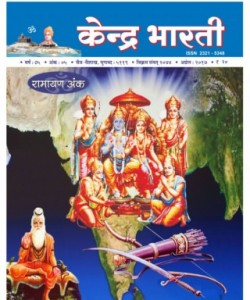राष्ट्र के रूप में हमारे पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। भारत के पास अत्यधिक उपजाऊ भूमि, अच्छी वर्षा, विशाल मानवीय संसाधन, बौद्धिक व तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, एक दीर्घ व सतत् इतिहास है तथा संघर्षरहित धर्म व दर्शनशास्त्र सजीव रूप में है। फिर भी हम विष्व के लिए दिशा निश्चित नहीं कर रहे हैं। वे जो ऐसा करते हैं, वे संस्कृति व विचारधारा की उपज हैं, जो असहिष्णुता, घृणा व हिंसा को जन्म देती है तथा दूसरों को अधीन करके उन पर शासन करने हेतु बाध्य करती है, क्यों ? क्योंकि हम बाह्य आक्रमण का वैचारिक व भौतिक दोनों प्रकार से सामना करने के लिए संगठित नहीं थे। हमने अपने वैष्विक स्थान को खो दिया तथा धीरे-धीरे राष्ट्र स्थान को भी, असहिष्ण विचारों तथा देशों के अधीन होकर खो दिया तथा अपने आप को शताब्दियों के लिए दासता में रखा। हम आन्तरिक समानता के लिए संगठित थे। यहाँ तक कि जो शत्रुओं के रूप में पहले आए थे, वे भी हमारे राष्ट्र व सांस्कृतिक जीवन द्वारा आत्मसात् व सम्मिलित कर लिए गए।
किन्तु जब अन्य जीवन पद्धतियाँ तथा पूजा पद्धतियों के प्रति असहिष्णुता का भाव रखने वाले शत्रु आए, तब उनका सामना करने की दृष्टि से हम संगठित नहीं थे। हमारी सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार के असहिष्णु विचारों से अपरिचित थी। वास्तव में एक राष्ट्र के रूप में, हमने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि इस प्रकार की असहिष्णुता भी अस्तित्व में है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि रोमन मूर्तिपूजक धर्म तथा रोमन राज्य स्वयं नष्ट हो गए क्योंकि वे नहीं जानते थे कि ऐसे असहिष्णु रिलिजन के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, जो अपने अतिरिक्त अन्य सभी पंथवादी विश्वासों को अस्वीकृत करता है। अर्थात् हम ऐसी पंथवादी निष्ठाओं से सर्वथा अपरिचित थे जो न केवल अन्य निष्ठाओं का अनादर करती है बल्कि उन्हें अस्वीकार भी करती है और यहाँ तक की अन्य निष्ठाओं को मिटाना अपना परम कर्तव्य समझती है। वास्तव में जब ऐसी पंथवादी (रिलीजियस) निष्ठाएँ पहली बार शरणार्थी के रूप में आई, जो ऐसे ही अन्य नि निष्ठाओं का शिकार हो गए थे या उनके ही अपने सह-नैष्ठिकों कों के द्वारा अधर्मी मान लिए गए थे, इस राष्ट्र ने ही उन्हें आश्रय तक दिया। इस प्रकार बहुत पहले से यहूदी, ईसाई, इस्लामी तथा पारसी समुदाय अन्य धर्मों या अपने सह-धर्मियों से सुरक्षा हेतु भारत में आकर बस गए। किन्तु जब वे जीतने हेतु आयी शक्तियों के रूप में आए, उस समय हमारी आन्तरिक व बाह्य, दोनों प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएँ, पर्याप्त व कुशल नहीं थी। किन्तु, चूँकि हमारी सभ्यता, राज्य तथा राष्ट्र पर निर्भर नहीं थी, इसलिए हम रोम तथा ग्रीक के समान नश्ट नहीं हुए, पर जीवित रहे, केवल जीवित रहे। यहाँ तक कि अभी भी हम केवल अनुजीवी ही है। स्वामीजी केवल जीवित भारत नहीं चाहते थे। वे एक जीवित हिन्दुत्व नहीं चाहते थे। वे एक ऐसा हिन्दुत्व तथा हिन्दू राष्ट्र चाहते थे, जो सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व करे, न कि विश्व में केवल अनुजीवी बनकर रहे।
जब से असहिष्णु ‘रिलीजन’ विचार तथा राष्ट्रों ने वैश्विक घटनाक्रमों में नेतृत्व करना प्रारम्भ किया तब से वैश्विक इतिहास तथा भूगोल बदल गए। इसलिए असहिष्णु विचारों तथा राष्ट्रों का सामना करने के लिए, पारम्परिक हिन्दू पद्धतियों को पुनः ढालने तथा समायोजित करने की आवश्यकता थी। यहीं से स्वामीजी ने संगठन पर बल देना शुरु किया। उनका हिन्दू समाज के लिए एक शब्द का मन्त्र था ‘संगठन ! संगठन !! जिसका अर्थ है एकता ! एकता !! क्या संगठन तथा एकता हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, स्वाभाविक नहीं ? क्या यह हमारी दृश्टि से पराई है ? जिन्होंने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में एकत्व देखा है क्या उनके लिए एकता की विशेषता, जो संगठन का आधार है, का न होना संभव है ? इसके लिए गम्भीर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मोक्ष (उसे ‘साल्वेशन’ बराबर मानकर) के हिन्दू-दृष्टिकोण का आधार यह है कि यह एक व्यक्तिगत प्रयास है तथा इसके लिए व्यक्तिगत रूप से समय देना भी आवष्यक है। वह व्यक्ति जो इसके लिए प्रयत्न करता है, उस समय मोक्ष प्राप्त करता है, जब वह इसके योग्य हो जाता है। यदि असफल होता है तो पुनः प्रयत्न करता है, सतत् प्रयत्न करता रहता है। मोक्ष के लिए हिन्दू धर्म में कोई सामूहिक प्रयास नहीं हो सकता, या मोक्ष हेतु सामूहिक समय नहीं हो सकता।
अब्रह्मिक पंथवादी निष्ठाओं में इससे विपरीत स्थिति है। विशेष रूप से ईसाई तथा इस्लाम रिलिजन में। ईसाइयों में परलोकशास्त्र की कल्पना, ईसाइयों के मोक्ष के विचार की व्याख्या करती है। वास्तव में, ईसाईवाद के अनुसार मोक्ष का समय सम्पूर्ण समुदाय के लिए है अर्थात् या तो सभी एक ही समय में मोक्ष प्राप्त करते हैं या सभी को मोक्ष प्रदान करने से एक साथ मनाकर दिया जाता है। अर्थात् ‘अॅपोकॅलिप्स’ की कल्पना के अनुसार वह वो समय है तब विश्व का अन्त होगा। जबकि हिन्दू अनादि-अनन्त में विश्वास करते हैं, ईसाइयों का विश्वास एकरेखीय समय रचना पर आधारित है, जिसके प्रारम्भ तथा अन्त का समय निश्चित बताया गया है। अन्त का समय अॅपोकॅलिप्स है ऐसा उनका विश्वास है। येशु के राज्य की स्थापना ईसाई विश्वास का केन्द्र है। विश्वास यह है कि ईसा वापस आएँगे तथा सम्पूर्ण विश्व पर एक हजार वर्षों तक शासन करेंगे। यह सहस्त्राब्दि की कल्पना है। अन्त समय तब आएगा, जब येशु के राज्य की स्थापना होगी तथा वे एक हजार वर्षों के लिए राज्य कर लेंगे, तब विश्व का अन्त हो जाएगा, अर्थात् समय का अन्त हो जाएगा। उस समय वे सभी ईसा जो हजारों वर्षों से दफनाएँ गए हैं, पुनः जीवन प्राप्त करेंगे तथा पृथ्वी व स्वर्ग के मध्य में पहुँचाये जाएँगे एवं उनके अच्छे व बुरे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और उसी के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नर्क प्रदान किया जाएगा अर्थात् सारे गैर-ईसाई जो पृथ्वी पर रहे हैं, वे नरक में ही जाएँगे। उस समय गैर-ईसाइयों के बचे रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर येशु का साम्राज्य तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि किसी ओर कोई भी गैर-ईसाई है।
इस प्रकार मोक्ष की ईसाई अवधारणा सामूहिक पर आधारित है। यह समूह का पंथवाद है, प्रार्थना में, अन्य धर्मों के प्रति व्यवहार में, ईसाईयों के प्रति व्यवहार में, पृथ्वी पर सभी को अपने साम्राज्य के अधीन करने में, प्रत्येक क्षेत्र में है। अतः ईश्वर के साम्राज्य के लिए, अन्य धार्मिक विश्वासों को मिटाने के लिए, सामूहिक प्रयासों को करने हेतु संगठित होना, यही येशु के साम्राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करने हेतु ईसाई पंथवाद का आन्तरिक व केन्द्रीय बिन्दु बन चुका है। यह सम्पूर्ण ईसाई सभ्यता का केन्द्र बन चुका है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, या आर्थिक क्षेत्र, समाज हो या पंथवाद। इस्लाम ने भी विश्व पर सामूहिक रूप से शासन करने के विचार को अपनाया तथा एक सामूहिक समय पर सिर्फ इस्लाम पर विश्वास करने वाले के लिए मोक्ष का आश्वासन दिया। राज्य स्वयं ही उनका सामूहिक यन्त्र था। ईसाई पंथवाद को राज्य प्राप्त करने के लिए चर्च की आवश्यकता पड़ी। इस्लाम को नहीं क्योंकि इस्लामी राज्य की स्थापना, इस्लाम पंथवाद की स्थापना का ही पर्याय था।
यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू कम संगठित थे या बिल्कुल भी संगठित नहीं थे, वास्तव में हिन्दू, धर्म के आधार पर अत्यधिक संगठित थे, जिसने उनके मन को संगठित किया था तथा यह उनके सामाजिक संगठन से प्रदर्शित होता था। संगठन की इस व्यवस्था ने किस प्रकार कार्य किया ? माननीय एकनाथजी ने ‘सेवा ही साधना’ में स्पष्ट किया है, ‘भारतीयों ने ही सर्वप्रथम सुसंगठित सामाजिक संस्था का सिद्धान्त प्रतिपादित किया तथा तदनुसार हजारों वर्षों तक एक संगठित समुदाय के रूप में जीवन-यापन करते रहे तथा इसे आज तक भी जारी रखा है, यद्यपि यह विकृत रूप में है, यह सिद्ध तथ्य है जो कि हिन्दू जीवनपद्धति की वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा प्रमाणित होता है। यदि आवश्यकता हो, तो अन्य साक्ष्य इस तथ्य को यह कहते हुए गुणित कर सकते हैं कि यज्ञ, जो ऋग्वैदिक आर्यों के हृदय का आदर्श था, सामूहिक धार्मिक पूजा के रूप में किया जाता था तथा इसमें सम्पूर्ण समाज सहभागी होता था, क्योंकि सम्पूर्ण ऋग्वेद में, एक भी ऐसी ऋचा मुश्किल से मिल सकती है, जहाँ किसी वस्तु की प्रार्थना या माँग, एक व्यक्ति के लिए की गई हो। यह सर्वदा ‘सभी के लिए’ है तथा ‘मैं’ के लिए नहीं। सर्वविदित गायत्री मन्त्र में, ‘हम सभी की बुद्धि प्रेरित करें’, इस हेतु प्रार्थना की गई है। दसवें मण्डल में ऋषि कहते हैं, ‘तुम सभी एक साथ जाओ, साथ में वार्तालाप करो तथा तुम सभी के मस्तिष्क एक साथ वस्तुओं को जानें’ इत्यदि (ऋग्वेद द 191-3-5) यजुर्वेद का महान् राष्ट्रगान सम्पूर्ण राष्ट्र तथा इसके विविध संगठनों का ही साथ वर्णन करता है, न कि व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति का। उपनिषदों के प्रसिद्ध शान्ति मन्त्र सम्पूर्ण समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं।’
परन्तु संगठन की इस तकनीक, प्रारूप व योजना की रचना बाह्य भय के कारण विश्व पर शासन करने के लिए नहीं की गई थी। यह आन्तरिक रचना को सुव्यवस्थित रखने के लिए थी। यह एकता गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से उस विकट कार्य के बराबर नहीं थी, जिसका सामना हिन्दुत्व को करना पड़ा जब अन्य धर्मों की वैधता को नकारने वाले विरोधी रिलिजन उभर आए। सृश्टि के एकत्व की हिन्दू संकल्पना उस परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसका सामना विश्व को, उस समय करना पड़ा, जब सृष्टि के एकत्व की संकल्पना को अमान्य करने वाले पंथवाद या निष्ठाएँ उभर आयी। अतः इसके स्थान पर एकता तथा संगठन के नये तथा मेल खाने वाले विचार को रखने की आवश्यकता थी।
हमारे अन्दर किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं थी इसलिए हम किसी के विरुद्ध संगठित नहीं थे। हम स्व-केन्द्रित थे, क्योंकि हमें कोई भय नहीं था। हम संगठित नहीं थे, क्योंकि हमें सामूहिक रूप से रक्षात्मक तथा आक्रामक होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम एक दूसरे के प्रति ईश्र्या भाव नहीं रखते थे, क्योंकि हमारे सामूहिक अस्तित्व को, किसी का कोई भय नहीं था। हम एक शान्तिपूर्ण व समृद्ध समाज के सभी परिणामों को बिना किसी बाह्य भय से भोग रहे थे। इसे एक परिवार के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि धनवान व समृद्ध है, जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति ईश्र्या भाव रखते हैं तथा इन बातों पर झगड़ते हैं कि प्रत्येक को क्या मिलना चाहिए तथा प्रत्येक के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। बाह्य आक्रमण झेलने से पूर्व, समृद्ध हिन्दू समाज की स्थिति यह थी।
बाह्य शक्तियों ने हमारी कमियों को उजागर कर दिया तथा साथ ही हमारी शक्ति व समृद्धि को कमजोर बना दिया तथा हमें उन गुणों को अर्जित करने के लिए बाध्य किया, जो हमारी प्रकृति के लिए नए थे, जैसे कि हमारा धर्म और जीवन-पद्धति की रक्षा के लिए नए तरीके से संगठित होना। जहाँ वे पंथवादी लोग अन्य लोगों को जीतने के लिए संगठित होते हैं, उसी प्रकार हमें भी संगठित होना लेकिन अपनी निष्ठा व धर्म की रक्षा के लिए। अध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टि से यह प्रयास श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द के दिव्य संयोग के साथ प्रारम्भ हुआ। स्वामीजी ने हिन्दुओं को निन्दायुक्त स्व आलोचना के द्वारा उत्तेजित कर उन्हें संगठित होने के लिए जागृत किया तथा उन आसुरी शक्तियों के द्वारा निर्मित भय की स्थिति का सामना करने हेतु एकत्रित होने को कहा, जो, इनसे असहमत लोगों पर विजय प्राप्तकर उन्हें नष्ट करने के लिए संगठित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप रामकृष्ण मिशन से शुरु होकर संगठनों का एक सतत् प्रवाह प्रारम्भ हुआ, जिनमें से प्रत्येक संगठन हिन्दू समाज की विभिन्न आवष्यकताओं को पूर्ण कर सके। इसी पूर्व-निर्धारित प्रवाह में, माननीय श्री एकनाथजी की संकल्पना तथा विचारों द्वारा, विवेकानन्द केन्द्र भी अस्तित्व में आया।
संगठन की भावना का मूल है कि सामूहिक ‘हम’ अर्थात् धर्म की पुनः स्थापना के लिए संगठन के हित में ‘मैं’ को नष्ट करना। एक साधक अपने अन्दर के ‘मैं’ को नष्ट करता है तथा अन्ततः अपने ‘मैं’ को परम सत्य में विलीन कर देता है। ठीक यही धर्म की पुनःस्थापना करने हेतु समर्पित संगठन का कार्यकर्ता करता है। धर्म की पुनःस्थापना के आदर्श का ही लगभग रूप है ऐसे संगठन की विशाल पहचान में कार्यकर्ता अपने ‘मैं’ को समाने की प्रक्रिया अपनाता है। संगठन ‘हम’ है, जिसमें वह अपने मैं, को समा देता है।